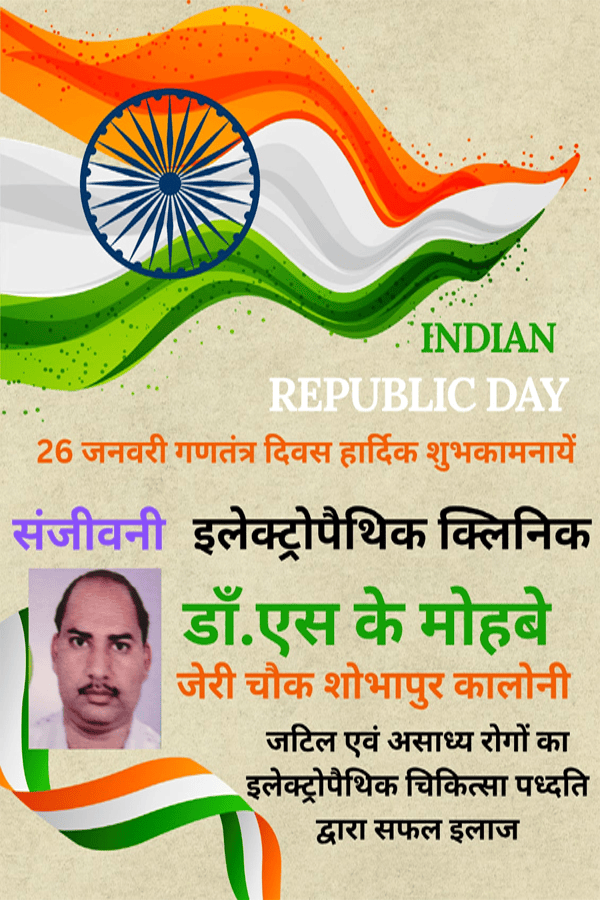उत्पिड़न और शोषण के खिलाफ मनुस्मृति दहन दिवस (25 दिसंबर 1927): एक विचार
उत्पिड़न और शोषण के खिलाफ मनुस्मृति दहन दिवस (25 दिसंबर 1927): एक विचार
 विश्व में धर्म को लेकर बहुत बड़े बड़े आंदोलन और विवाद हुए हैं। धर्म पुस्तक को लेकर भी विवाद रहा है। उसी कड़ी में दो नाम ऐसे हैं जिनके साहसिक कदम ने पूरे समाज को बदलने के लिए मजबूर कर दिया। जर्मनी के मार्टिन लूथर और भारत के अंबेडकर में एक जैसी समानता थी, दोनों ही व्यक्ति ने धर्म को चुनौती दी। एक ओर जहां मार्टिन लूथर ने 31अक्टूबर 1517 को पोप के द्वारा प्रतिपादित पाप मोचन बेचने का विरोध किया और अपनी पंचानवे थेसिस विटनबर्ग के कैसल गिरजाघर के प्रवेश द्वार पर लिखकर पोप को बहस के लिए चुनौती दी वहीं, अंबेडकर ने हिंदू के धर्म ग्रंथ मनुस्मृति को 25 दिसंबर 1927 को महाराष्ट्र के कोलाबा जिले के महाड़ में सार्वजनिक रूप से जलाया और बाद में संविधान लिखा। दोनों ही घटनाएं एक जैसी नहीं है, परंतु दोनों ही धर्म से जुड़ी घटनाएं जरूर हैं। समाज में प्रचलित धारणाओं और मान्यताओं को चुनौती देने वालीं दोनों ही घटनाएं साहसिक और प्रेरणदायी कदम जरूर था। आधुनिक औपनिवेशिक इतिहास में महात्मा फुले ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने मनुस्मृति में व्याप्त उल्लेख को सर्वप्रथम चुनौती दी। उनकी यह परंपरा आगे चलकर अंबेडकर के द्वारा पूर्ण हुई। धार्मिक मान्यता और धर्म पुस्तक में उद्धरित बातें, मनुष्य को मानसिक रूप से गुलाम बनाने का काम करती है। यह पूरी दुनिया में सर्वविदित है, भारत इससे अछूता नहीं था। जिस प्रकार यूरोप में पोप हर किसी व्यक्ति के किए गए कर्म को पाप समझकर उसे पैसे लेकर माफ कर देता था, वैसे ही भारत में मनुस्मृति में समाज में दलितों को और महिलाओं को किस प्रकार वश में किया जाए यह एक पुस्तक के द्वारा संचालित होता था। समाज का पूरा ताना बाना इसी पुस्तक से संचालित हो रहा था, जिसका दुष्परिणाम खासकर दलित और महिलाओं के लिए चिंतनीय था। इस घटना को 25 दिसंबर 1927 को अंजाम दिया गया जो कि आगे चलकर मील का पत्थर साबित हुआ। इस मायने में अंबेडकर मार्टिन लूथर किंग से एक कदम आगे जाकर प्रतीकात्मक तरीके से मनुस्मृति का दहन किया और हिंदू धर्म के ठेकेदारों को सामने से चुनौती दी। यह एक साहसिक और सराहनीय कदम था, जो सदियों से समाज को जकड़ा हुआ था। भारत जैसे देश में जहां जातिवाद पूरी तरह से हावी था और वह मनुस्मृति पर आधारित समाज काम कर रहा था, उस पुस्तक का दहन कर अंबेडकर ने समाज को एक संदेश देने का काम किया। कोई भी धर्म पुस्तक कानून का रूप कैसे ले सकता है? अंबेडकर ने आखिर मनुस्मृति को ही क्यों चुना? मनुस्मृति में ऐसी क्या बातें थी जो अंबेडकर उसे जलाने को आतुर थे? उनसे पहले के सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों में इसकी चर्चा क्यों नहीं हुई? आखिर ब्रिटिश काल में ही इस पुस्तक को पूरी तरीके से जलाने का काम क्यों किया गया? इसके पहले किसी महापुरुष ( फुले को छोड़कर) को यह आभास और एहसास क्यों नहीं हुआ आखिर यह धर्म पुस्तक कानून का रूप कैसे ली हुई थी? इसमें ऐसी क्या बातें लिखी गई थी जिसका पालन सभी लोग शांतिपूर्वक और बिना कोई विरोध किए हुए कर रहे थे? लोग चुपचाप इस धर्म ग्रंथ को कानून का किताब मानकर क्यों सहन कर रहे थे? क्या इसके बिना हमारा समाज नहीं चल सकता था? क्या इसके लिए इस धार्मिक पुस्तक का होना जरूरी था? आखिर किसी ने आज तक विरोध क्यों नहीं जताया? एक बात और गौर करने के लायक है की अंबेडकर खुद ही पुस्तक प्रेमी थे। उन्होंने खुद ही विदेशों और भारत में किताब को संग्रहित करने का काम किया और उसे पढ़कर समाज को रास्ता दिखाया। पुस्तक में लिखे विचार, बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। इस बात का आभास अंबेडकर को पहले से था क्योंकि महात्मा फूले के पुस्तकों और विचारों को पढ़ और जानकर ही इस क्रांतिकारी कदम को अख्तियार किया था। धार्मिक पुस्तकें अगर जाति, लिंग और भेदभाव पर आधारित हो तो कोई भी व्यक्ति उसे पढ़कर उद्वेलित होगा। फिर उन्होंने इस पुस्तक को जलाने के लिए ही क्यों चुना? अंबेडकर ने सामाजिक आंदोलन को अंजाम देते हुए मनुस्मृति जलाने का ही फैसला क्यों किया? क्या मनुस्मृति को जलाने से समाज में परिवर्तन आया? आखिर इसका चुनाव उन्होंने खुद किया या किसी के कहने पर किया? कई सारे सवाल मन में उठते हैं और जाहिर सी बात है अंबेडकर के मन में भी इस पुस्तक को जलाने से पहले उठे होंगे। आख़िर अपने उस सवालों का जवाब उन्हें नहीं मिला होगा और तभी इसे जलाने के लिए विवश हुए होंगे। जब व्यक्ति किंकर्तव्यविमूढ हो जाता है और चारों ओर से सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तभी इस तरह के कठोर कदम उठाए जाते हैं। अंबेडकर ने भी अपने बाल्यकाल से इस जातिदंश को झेला था और विदेश में पढ़ाई करने और सर्वोच्च डिग्री हासिल होने के बावजूद उन्हें सामाजिक और धार्मिक विद्वेष झेलना पड़ रहा था। उन्होंने अपने आसपास और समाज में घट रही जातीय और धार्मिक भेदभाव को बिल्कुल करीब से देखा, सहा और फिर विद्रोह का रूप तैयार किया। दलित और दमित व्यक्तियों के साथ पशु से भी खराब व्यवहार किया जाता था। यह उनका कोई व्यक्तिगत एजेंडा नहीं था बल्कि समाज के वह हर दलित, दमित और कुत्सित समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। आखिर व्यक्ति जब अपने से ऊपर समाज को देखता है तो कई सारी विसंगतियां एक साथ नजर आती है। उन विसंगतियों को दूर करने के लिए कुछ साहसिक कदम की जरूरत होती है। ऐसा कदम जो समाज को स्वीकार्य हो और जिसका दूरगामी परिणाम निकले।
विश्व में धर्म को लेकर बहुत बड़े बड़े आंदोलन और विवाद हुए हैं। धर्म पुस्तक को लेकर भी विवाद रहा है। उसी कड़ी में दो नाम ऐसे हैं जिनके साहसिक कदम ने पूरे समाज को बदलने के लिए मजबूर कर दिया। जर्मनी के मार्टिन लूथर और भारत के अंबेडकर में एक जैसी समानता थी, दोनों ही व्यक्ति ने धर्म को चुनौती दी। एक ओर जहां मार्टिन लूथर ने 31अक्टूबर 1517 को पोप के द्वारा प्रतिपादित पाप मोचन बेचने का विरोध किया और अपनी पंचानवे थेसिस विटनबर्ग के कैसल गिरजाघर के प्रवेश द्वार पर लिखकर पोप को बहस के लिए चुनौती दी वहीं, अंबेडकर ने हिंदू के धर्म ग्रंथ मनुस्मृति को 25 दिसंबर 1927 को महाराष्ट्र के कोलाबा जिले के महाड़ में सार्वजनिक रूप से जलाया और बाद में संविधान लिखा। दोनों ही घटनाएं एक जैसी नहीं है, परंतु दोनों ही धर्म से जुड़ी घटनाएं जरूर हैं। समाज में प्रचलित धारणाओं और मान्यताओं को चुनौती देने वालीं दोनों ही घटनाएं साहसिक और प्रेरणदायी कदम जरूर था। आधुनिक औपनिवेशिक इतिहास में महात्मा फुले ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने मनुस्मृति में व्याप्त उल्लेख को सर्वप्रथम चुनौती दी। उनकी यह परंपरा आगे चलकर अंबेडकर के द्वारा पूर्ण हुई। धार्मिक मान्यता और धर्म पुस्तक में उद्धरित बातें, मनुष्य को मानसिक रूप से गुलाम बनाने का काम करती है। यह पूरी दुनिया में सर्वविदित है, भारत इससे अछूता नहीं था। जिस प्रकार यूरोप में पोप हर किसी व्यक्ति के किए गए कर्म को पाप समझकर उसे पैसे लेकर माफ कर देता था, वैसे ही भारत में मनुस्मृति में समाज में दलितों को और महिलाओं को किस प्रकार वश में किया जाए यह एक पुस्तक के द्वारा संचालित होता था। समाज का पूरा ताना बाना इसी पुस्तक से संचालित हो रहा था, जिसका दुष्परिणाम खासकर दलित और महिलाओं के लिए चिंतनीय था। इस घटना को 25 दिसंबर 1927 को अंजाम दिया गया जो कि आगे चलकर मील का पत्थर साबित हुआ। इस मायने में अंबेडकर मार्टिन लूथर किंग से एक कदम आगे जाकर प्रतीकात्मक तरीके से मनुस्मृति का दहन किया और हिंदू धर्म के ठेकेदारों को सामने से चुनौती दी। यह एक साहसिक और सराहनीय कदम था, जो सदियों से समाज को जकड़ा हुआ था। भारत जैसे देश में जहां जातिवाद पूरी तरह से हावी था और वह मनुस्मृति पर आधारित समाज काम कर रहा था, उस पुस्तक का दहन कर अंबेडकर ने समाज को एक संदेश देने का काम किया। कोई भी धर्म पुस्तक कानून का रूप कैसे ले सकता है? अंबेडकर ने आखिर मनुस्मृति को ही क्यों चुना? मनुस्मृति में ऐसी क्या बातें थी जो अंबेडकर उसे जलाने को आतुर थे? उनसे पहले के सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों में इसकी चर्चा क्यों नहीं हुई? आखिर ब्रिटिश काल में ही इस पुस्तक को पूरी तरीके से जलाने का काम क्यों किया गया? इसके पहले किसी महापुरुष ( फुले को छोड़कर) को यह आभास और एहसास क्यों नहीं हुआ आखिर यह धर्म पुस्तक कानून का रूप कैसे ली हुई थी? इसमें ऐसी क्या बातें लिखी गई थी जिसका पालन सभी लोग शांतिपूर्वक और बिना कोई विरोध किए हुए कर रहे थे? लोग चुपचाप इस धर्म ग्रंथ को कानून का किताब मानकर क्यों सहन कर रहे थे? क्या इसके बिना हमारा समाज नहीं चल सकता था? क्या इसके लिए इस धार्मिक पुस्तक का होना जरूरी था? आखिर किसी ने आज तक विरोध क्यों नहीं जताया? एक बात और गौर करने के लायक है की अंबेडकर खुद ही पुस्तक प्रेमी थे। उन्होंने खुद ही विदेशों और भारत में किताब को संग्रहित करने का काम किया और उसे पढ़कर समाज को रास्ता दिखाया। पुस्तक में लिखे विचार, बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। इस बात का आभास अंबेडकर को पहले से था क्योंकि महात्मा फूले के पुस्तकों और विचारों को पढ़ और जानकर ही इस क्रांतिकारी कदम को अख्तियार किया था। धार्मिक पुस्तकें अगर जाति, लिंग और भेदभाव पर आधारित हो तो कोई भी व्यक्ति उसे पढ़कर उद्वेलित होगा। फिर उन्होंने इस पुस्तक को जलाने के लिए ही क्यों चुना? अंबेडकर ने सामाजिक आंदोलन को अंजाम देते हुए मनुस्मृति जलाने का ही फैसला क्यों किया? क्या मनुस्मृति को जलाने से समाज में परिवर्तन आया? आखिर इसका चुनाव उन्होंने खुद किया या किसी के कहने पर किया? कई सारे सवाल मन में उठते हैं और जाहिर सी बात है अंबेडकर के मन में भी इस पुस्तक को जलाने से पहले उठे होंगे। आख़िर अपने उस सवालों का जवाब उन्हें नहीं मिला होगा और तभी इसे जलाने के लिए विवश हुए होंगे। जब व्यक्ति किंकर्तव्यविमूढ हो जाता है और चारों ओर से सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तभी इस तरह के कठोर कदम उठाए जाते हैं। अंबेडकर ने भी अपने बाल्यकाल से इस जातिदंश को झेला था और विदेश में पढ़ाई करने और सर्वोच्च डिग्री हासिल होने के बावजूद उन्हें सामाजिक और धार्मिक विद्वेष झेलना पड़ रहा था। उन्होंने अपने आसपास और समाज में घट रही जातीय और धार्मिक भेदभाव को बिल्कुल करीब से देखा, सहा और फिर विद्रोह का रूप तैयार किया। दलित और दमित व्यक्तियों के साथ पशु से भी खराब व्यवहार किया जाता था। यह उनका कोई व्यक्तिगत एजेंडा नहीं था बल्कि समाज के वह हर दलित, दमित और कुत्सित समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। आखिर व्यक्ति जब अपने से ऊपर समाज को देखता है तो कई सारी विसंगतियां एक साथ नजर आती है। उन विसंगतियों को दूर करने के लिए कुछ साहसिक कदम की जरूरत होती है। ऐसा कदम जो समाज को स्वीकार्य हो और जिसका दूरगामी परिणाम निकले।
मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय हैं, जिनमें 2684 श्लोक हैं कुछ संस्करण में इसकी संख्या 2964 भी है। यह श्लोक बहुजन समाज और महिलाओं के प्रति दासता की जीवंतता को बताती और दर्शाती है। यह भेदभाव और जाति आधारित कानून की पुस्तक समाज में आपसी वैमनस्यता को बताती है। किस जाति के लोगों को क्या करना है, उन पर किस तरह का प्रतिबंध होगा,व्याह बताने का काम करती है। जाहिर सी बात है गुलामी और दासता का यह दस्तावेज कहीं से भी समाज को अग्रसित दिशा में नहीं ले जाने वाली थी।
मनुस्मृति की होली जलाने के बारे में बोलते हुए, अंबेडकर ने 1938 में टी वी परवते के साथ एक साक्षात्कार में कहा था ” मनुस्मृति की होली जलाना नितांत साभिप्राय था। हमने इसकी होली इसलिए जलाई की हम इसे उस अन्याय का प्रतीक समझते हैं जिसके नीचे हम सदियों से पिसते आए हैं। इसके उपदेशों के कारण हम घृणित निर्धनता के नीचे पिसते आए हैं और इसलिए हमने विरोध किया, सब कुछ दांव पर लगा दिया। हथेली पर जान रख दी और कार्य को पूरा किया।”(बाबासाहेब सम्पूर्ण वांग्मय, खंड ३५, पृष्ठ संख्या २६) अंबेडकर ने अपने विरुद्ध लगाए गए आरोप का जवाब बहिष्कृत भारत में विस्तारपूर्वक लिखा। उनका मानना था कि ” मनुस्मृति अछूत हिन्दुओं की कथित उच्च वर्ग के हिन्दुओं द्वारा दीर्घकाल से किए जा रहे उत्पीड़न और शोषण का आदेश देती है और उसे उचित ठहराती है, वर्तमान हिन्दू कानून का यह मुख्य स्रोत जलाए जाने योग्य है।”(पृष्ठ संख्या ३१)